जम्मू-कश्मीर : जम्हूरियत, कश्मीरियत, ना ही इंसानियत
मुद्दा सिर्फ इस संवेदनशील राज्य में शासन को, जहां जनता के बड़े हिस्से का वैसे भी भारत सरकार से गहरा अलगाव हो चुका है, एक निर्वाचित सरकार की वैधता से लंबे समय तक वंचित रखे जाने का ही नहीं है,
Trending now

मोदी-2 में भारत में उत्तर-सत्य युग बाकायदा शुरू हो गया है। जम्मू-कश्मीर मेंराष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव के पक्ष में नये गृहमंत्री, अमित शाह ने जो कुछ कहा और करने का इरादा जताया, कम से कम कश्मीर के संदर्भ में तो जैसे इस नये युग के आरंभ का ही एलान था। मौजूदा शासन ने, हर चीज के, हर धारणा के, अर्थ पूरी तरह से बदल ही दिए हैं। जिन चीजों को अब तक अमूल्य समझा जाता था, उन्हें मामूली बना दिया गया है और जिन्हें स्वीकृत सत्य मानकर चला जाता था, उन्हें सिरे से अमान्य कर दिया गया है। इसीलिए, 17वीं लोकसभा में अपने पहले ही किंतु बहुत ही हमलावर तथा टकराववादी भाषण के दौरान अमित शाह ने जब जम्मूू-कश्मीर के साथ सलूक के संदर्भ में एनडीए के पहले प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी का ‘‘जम्हूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत’’ का सूत्र दुहराया, तो यह उनकी सरकार की बुनियादी तौर पर ‘ताकत दिखाऊ’ नीति के साथ, वाजपेयी का सूत्र दुहराए जाने की विडंबना तक ही सीमित नहीं रहा। जैसाकि कई टिप्पणीकारों ने दर्ज भी किया, मोदी-2 के गृहमंत्री वास्तव में वाजपेयी के बहुउद्यृत सूत्र को ही इस तरह पुनर्परिभाषित कर रहे थे कि उसे भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार की ‘ताकत दिखाऊ नीति’ की हिमायत के लिए, सिर के बल खड़ा किया जा सके।
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए और बढ़ाने का शाह का प्रस्ताव अपने आप में उत्तर-सत्य का अच्छा उदाहरण था। बेशक, जम्मू-कश्मीर में न तो राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया है और न ही उसका विस्तार पहली बार हो रहा है। उल्टे जम्मू-कश्मीर शायद देश का ऐसा राज्य है, जो आजादी के बाद से सबसे ज्यादा अर्से तक राज्यपाल/ राष्ट्रपति शासन में रहा है। इस राज्य के अशांत हालात के साथ जुडक़र ऐसा होना कम से कम शेष भारत के लोगों के लिए इतना सामान्य हो चुका है कि इस प्रस्ताव का शायद ही कोई खास विरोध देखने को मिला, न संसद में और न संसद के बाहर। और मामूली बहस के बाद, संसद के दोनों सदनों ने राज्य में राष्टï्रपति शासन की अवधि छह महीने के लिए और बढ़ाने का अनुमोदन भी कर दिया। वैसे भी, शुक्रवार 28 जून को जब केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा राष्ट्रपति शासन के विस्तार का प्रस्ताव पेश किया गया, इस प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना एक तरह से संवैधानिक बाध्यता ही बन चुका था। हफ्ते भर में ही राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि पूरी होने जा रही थी और चूंकि तब तक चुनाव किसी भी तरह से हो ही नहीं सकते थे, अगर जम्मू-कश्मीर को लेकर संवैधानिक संकट नहीं खड़ा होना था तो, राष्ट्रपति शासन का विस्तार अपरिहार्य था।
लेकिन, समस्या राष्ट्रपति शासन के विस्तार में उतनी नहीं है, जितनी कि गृहमंत्री द्वारा राज्यपाल/ राष्ट्रपति शासन को एक समस्या या मजबूरी के रास्ते के रूप में पेश किए जाने की जगह, जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत ही कारगर व्यवस्था के रूप में पेश किए जाने में है। बेशक, शाह ने न सिर्फ यह दावा किया कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर में कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार है बल्कि अपने भाषण के आखिर में साल के आखिर तक राज्य में चुनाव करा लिए जाने का भरोसा भी जताया। यह दूसरी बात है कि इसके सवालों के जवाब में कि जब संसद के चुनाव शांतिपूर्वक कराए जा सकते थे, तो विधानसभाई चुनाव क्यों नहीं कराए गए और विधानसभा चुनाव फौरन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर डाल दी कि चुनाव कब कराना है, यह तय करना उसका काम है। लेकिन, यह असुविधाजनक सवालों से बचने के लिए झूठी बहानेबाजी भर है क्योंकि जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य में चुनाव आयोग सुरक्षा की स्थिति के संबंध में सरकार के परामर्श के आधार पर ही चुनाव की तारीखें तय कर सकता है, उससे स्वतंत्र रूप से नहीं।
बहरहाल, मुद्दा सिर्फ चुनाव की तारीखों का नहीं है। मुद्दा सबसे पहले तो यही है कि राज्य में विधानसभा भंग किए जाने की नौबत आयी ही क्यों? क्यों उसके बाद भी, ओडिशा व आंध्र की तरह, संसद के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी नहीं कराए गए, जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन का विस्तार जरूरी हो गया था? यहां यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि 2014 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद, जम्मू पर केंद्रित अपनी हिंदुत्ववादी गोलबंदी के बल पर, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद, इस राज्य में पहली बार सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा ने, क्षेत्रीय पार्टी पीडीपी के साथ, सरासर अवसरवादी गठजोड़ किया था, जिसका अपने बढ़ते हुए अंतर्विरोध के चलते ज्यादा चल पाना संभव ही नहीं था। सीधे जम्मू में अपना हिंदुत्ववादी आधार मजबूत करने और कश्मीरियों के असंतोष से बिना किसी रू-रियायत के सख्ती से निपटने की मोदी सरकार की छवि के जरिए, शेष देश भर में भी अपने हिंदुत्ववादी आधार को पुख्ता करने की अपनी कार्यनीति के हिस्से के तौर पर भाजपा ने, लगभग ढाई साल में ही समर्थन वापस लेकर इस गठबंधन सरकार को गिरा दिया।
लेकिन, इसके बाद भी फौरन विधानसभा को भंग नहीं किया गया, जिसकी कि अन्य सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मांग कर रही थीं। इसके बजाए, राज्य विधानसभा को निलंबित कर के रखा गया, ताकि जोड़-तोड़ से सरकार बनायी जा सके। वास्तव में पिछले साल के आखिरी महीनों में जोड़-तोड़ से अपनी एक जेबी सरकार बैठाने की भाजपा ने बाकायदा कोशिश भी की थी। लेकिन, ऐन मौके पर राज्य की प्रमुख गैर-भाजपा पार्टियों, पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस तथा कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने की पेशकश कर दी, जिसे विधानसभा में विधायकों के स्पष्टï बहुमत का समर्थन हासिल था। बहरहाल, भाजपा द्वारा इस बीच राज्यपाल बनाकर लाए गए उसके एक पूर्व-नेता, सत्यपाल मलिक ने नाटकीय तरीके से इस गठबंधन के सरकार बनाने के दावे के लिए अपने दरवाजे ही बंद कर लिए और जल्दी-जल्दी में राज्य विधानसभा की भंग करने की घोषणा कर दी। इस तरह, जम्मू-कश्मीर में गैर-भाजपा सरकार नहीं बनने देने के भाजपा और उसकी केंद्र सरकार के क्षुद्र राजनीतिक खेल की वजह से ही, जम्मू-कश्मीर को चुनी हुई सरकार से वंचित नहीं रहना पड़ा है, राज्यपाल के राज और फिर राष्ट्रपति शासन की छह महीने की अवधि पूरी होने के बाद, अब छह महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन का विस्तार किया गया है।
बहरहाल, मुद्दा सिर्फ इस संवेदनशील राज्य में शासन को, जहां जनता के बड़े हिस्से का वैसे भी भारत सरकार से गहरा अलगाव हो चुका है, एक निर्वाचित सरकार की वैधता से लंबे समय तक वंचित रखे जाने का ही नहीं है, हालांकि इससे हालात का और बिगडऩा स्वयंसिद्घ है। इससे ज्यादा बुनियादी मुद्दा गृहमंत्री के माध्यम से मौजूदा सरकार के यह दावा कर रहे होने का है कि राज्यपाल/ राष्टï्रपति शासन में राज्य में हालात में बहुत सुधार हुआ है और उससे पहले राज्य में रही पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार समेत, सभी चुनी हुई सरकारों के कार्यकाल के मुकाबले, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। चूंकि भाजपा जम्मू-कश्मीर को सबसे बढकऱ राष्ट्रीय सुरक्षा’ की नजर से ही देखती है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि शाह की नजर में, जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल/ राष्ट्रपति शासन, किसी चुनी हुई सरकार के मुकाबले, राष्ट्र के हित में बेहतर विकल्प है। हां! अगर वहां चुनाव के जरिए सीधे भाजपा द्वारा संचालित सरकार बन सकती हो तो बात दूसरी है। लेकिन, उससे कम भाजपा को मंजूर नहीं है। आखिरकार, पीडीपी के नेतृत्व वाली खुद अपनी पार्टी की गठबंधन सरकार के मुकाबले, हालात में राष्ट्रहित में भारी सुधार का दावा तो अमित शाह कर ही रहे थे! जनतंत्र और राष्ट्र हित माने, केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का राज! उसके लिए मोदी-शाह सरकार कुछ भी करेगी। सांप्रदायिक धु्रवीकरण के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश से लेकर, दूसरी पार्टियों या उनके विधायकों की खरीद-फरोख्त या राष्ट्रपति/ राज्यपाल शासन के नाम पर सीधे नई-दिल्ली से शासन तक, शब्दश: सब कुछ। यही है जम्हूरियत की उनकी नयी परिभाषा!
और कश्मीरियत! कश्मीरियत की शाह की सरकार को कितनी परवाह है, इसका अंदाजा सिर्फ एक इशारे से लगाया जा सकता है। गृहमंत्री की हैसियत से अपनी जम्मू-कश्मीर की पहली यात्रा में शाह ने क्या किया? उन्होंने एक ओर तो बहुप्रचारित तरीके से अधिकारियों के साथ बैठकें कर, उनकी इस यात्रा के कुछ ही दिनों में शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। और दूसरी ओर, उतने ही प्रचारित तरीके से, कश्मीर में किसी भी राजनीतिक पहल, राजनीतिक शक्तियों के साथ संवाद की किसी भी प्रक्रिया की जरूरत को, नकार दिया। भारत के किसी गृहमंत्री की जम्मू-कश्मीर की यात्रा में इससे कभी ऐसा नहीं हुआ था। यह सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी संकेत इसलिए और भी महत्वपूर्ण था कि गृहमंत्री की राज्य की पहली यात्रा की पूर्वसंध्या में और संभवत: उसकी तैयारी के रूप में, राज्यपाल सतपाल मलिक ने, सार्वजनिक रूप से यह जानकारी दी थी कि अलगाव की मांग करने वालों में से उदारपंथी धड़ा, सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। बहरहाल, शाह ने साफ कर दिया कि उनकी कोई संवाद शुरू करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है।
जाहिर है कि यह निजी दिलचस्पी होने न होने का मामला नहीं है। इसके जरिए भाजपा, आम तौर पर कश्मीर के बाहर देश भर में और खासतौर पर जम्मू में, अपने हिंदू समर्थकों को यही संदेश देना चाहती है कि उसे कश्मीरियों की की परवाह नहीं है। इसी संदेश को खतरनाक तरीके से आगे बढ़ाते हुए, गृहमंत्री की कश्मीर यात्रा के बाद, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के नाम पर पहली बार, यात्रा के काफिलों के चलने के समय पर यात्रा रूट पर, कश्मीरवासियों के लिए एक तरह के कफ्र्यू ही लगा दिया गया। यह पुलवामा की घटना के बाद से, सुरक्षा बलों के काफिलों की हिफाजत के नाम पर, उनके रूट पर नागरिकों के लिए लगाए गए यात्रा कफ्र्यू का ही विस्तार था। इस तरह, अमरनाथ यात्रा को, जिसका कश्मीर में किसी भी गुट ने कभी विरोध नहीं किया है और आम तौर पर कश्मीरी दिल खोलकर स्वागत ही करते आए हैं, एक तरह से सुरक्षाबलों की दमनकारी छवि देने की ही कोशिश की गयी है। यह सबसे बढकऱ जम्म-कश्मीर के लिए अमरनाथ यात्रा की मुख्यत: सांस्कृतिक परंपरा को, सांप्रदायिक हथियार बनाने की कोशिश है।
लेकिन, इसमें शायद ही किसी को अचरज होगा। यह एक जानी-मानी बात है कि भाजपा ने इस राज्य में मुस्लिम कश्मीर बनाम हिंदू जम्मू के विभाजन के जरिए अपने पांव फैलाए हैं और अब आने वाले विधानसभाई चुनाव के लिए, वे चाहे जब भी कराए जाएं, इसी खाई को और चौड़ा करने के आसरे है। अचरज नहीं कि भाजपा अखिल भारतीय स्तर पर ही नहीं जम्मू में भी, राज्य की स्वायत्तता से लेकर, उसके विशेष दर्जे पर मोहर लगानेवाली संविधान की धारा-370 तक, इस राज्य के वृहत्तर हितों की रक्षा की हरेक मांग के खिलाफ है। इस तरह क्षेत्रीय से बढक़र सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने में लगी भाजपा, कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को सांप्रदायिक रूप से भुनाने के सिवा, किस कश्मीरियत की बात सकती है? शाह के मुंह से कश्मीर की सूफी परंपरा की दुहाई सुनना तो जैसे शैतान के मुंह से धर्मग्रंथ का पाठ सुनना ही था।
सभी जानते हैं कि कश्मीरियों के साथ (पाकिस्तान प्रति रुख उसी का सीमा-पार विस्तार है) बिना किसी रू-रियायत के सख्ती से पेश आने की मोदी सरकार की नीति, उक्त ध्रुवीकरण के जरिए भाजपा के जनाधार को पुख्ता करने के लिए जरूरी है। अचरज की बात नहीं है कि संसद में अमित शाह के भाषण में सबसे ज्यादा जोर कश्मीर में विरोधियों के ‘दिलों में डर’ बैठाने पर ही था। यह इसके बावजूद है कि मोदी सरकार द्वारा अपनायी गयी तथाकथित ‘‘जीरो टॉलरेंस’’ की नीति ने अगर मारे जाने वाले मिलिटेंटों की संख्या में स्पष्टï बढ़ोतरी की है, तो इन मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों की जवानों और नागरिकों की मौतों में भी, वैसी ही उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। यही है इंसानियत के उनके दावे की हकीकत। सभी जानते हैं कि इस नीति की कामयाबी के मौजूदा सरकार के दावों के उलट, सचाई यही है कि कश्मीर की घाटी में जनता का अलगाव ही शीर्ष पर नहीं पहुंच गया है, स्थानीय नौजवानों के मिलिटेंट बनने की रफ्तार में भी जबर्दस्त तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साफ है कि यह नीति गोलियों का खर्चा और लाशों की संख्या ही बढ़ा सकती है, बढ़ा रही है। लेकिन, इसी तर्क से इसे राष्ट्र हित का तकाजा बताया जा रहा है। यही तो उत्तर-सत्य युग है।
लेखक-साप्ताहिक अखबार लोकलहर के संपादक है।
© 2017 - ictsoft.in

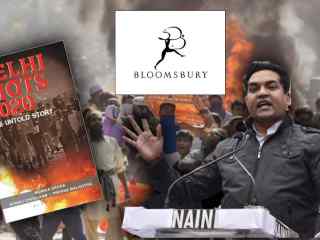














Leave a Comment