किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में। प्रगति-मैदान जाने का भी वह पहला मौका था। वास्तुकार चाल्र्स कोरिया की रचित त्रिकोणीय भवनों और किताबों के जखीरे को देख अभिभूत था
Trending now

बरस 1996 में दिल्ली में भटकते हुए मैं अनायास प्रगति मैदान में चला गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में। प्रगति-मैदान जाने का भी वह पहला मौका था। वास्तुकार चाल्र्स कोरिया की रचित त्रिकोणीय भवनों और किताबों के जखीरे को देख अभिभूत था। कस्बाई पुस्तक मेले मैंने देख रखे थे। विविध भाषाओं और अनुशासनों की इतनी सारी किताबें कि वाह! अतिउत्साह में जेब और जरुरतों का अतिक्रमण करते हुए मैंने किताबें खरीद डाली थीं।
बीते बीस-बाईस बरसों में होते आये मेलों का अमूमन दर्शक-ग्राहक रहा हूं। पहले दो बरसों के अंतराल पर यह भरता था। अब हर साल होने लगा है। हमारा भारतीय मानस मेलो-ठेलों में रमता है। भटकना, मिलना-जुलना, गपियाना, हंसी-ठिठोली करना और ठहाके लगाना हमारे मिजाज में होता है। पुस्तक-मेला आखिर मेला ही है, अपवाद नहीं। किताबें बेचने-खरीदनें, नई किताबों का लोकार्पण करने, कुछ किताबों या सामयिक साहित्यिक मसलों पर चर्चा करने के अलावा इस मेले में कुछ और नहीं होता?
रचनात्मकता से इतर अनेक तिकड़मों, जोड़-जुगाड़ों और उठा-पटक के लिए भी यह मेला चर्चा में रहता है। कहते हैं जहां चार लोग इकठठा होंगे, यह सब भी होगा। बहरहाल, सोशल-मीडिया के इस दौर में निजता दूर की कौड़ी हुई जा रही है। हर हरकत पलक झपकते ही सार्वजनिक दायरे में है। त्वरितता और तात्कालिकता पर बड़ा जोर है। सोशल मीडिया पर इधर मेले की चर्चाएं रहीं। हिंदी साहित्य में अपनी उपलब्धियों या यार-दोस्तों से मेल-मिलाप करते लोग हैं तो उनकी खिल्ली उड़ाने वाले भी हैं। मेले में न जा पाने का मलाल करने वाले भी है तो मेले में न जाने की ठाने बैठे लोग भी हैं। अपनी-अपनी सोच और चयन का मामला है।
सवाल यह है कि मेले के बाहर क्या जोड़-तोड़, आत्म-प्रदर्शन, चिरौरियां और साजिशें नहीं हैं ?
तीस से अधिक बरसों से हिंदी साहित्य पढऩे-जानने की कोशिश करता रहा हूं। एक चौथाई सदी से शक्ति संपन्न व्यक्तियों, सरकारी व निजी संस्थाओं, असंगठित समूहों और विचारधारात्मक संगठनों को दूर-पास से देखने-समझने के मौके भी पर्याप्त मिले हैं। साहित्य में पूंजी के वर्चस्व के समक्ष शरणागत होते नवागतों तो क्या ख्यातनामों को भी देखा है। सत्ता, सम्मान, साधन आदि पा जाने के लिये कैसी खींचतान चलती है, उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। किस तरह किसी को बढ़ाया और किसी को छांटा जाता है, इसके कई उदाहरण जानता हूं। साधनों के भरोसे कैसे दोयम दर्जे का रचनाकार भी कालजयी हो जाने का गुमान पाल लेता है, इसके प्रमाण भी इफरात में मौजूद हैं।
यह कोई रहस्य नहीं है कि ना जाने किन-किन शहरों-कस्बों-गांवों में हिंदी साहित्य की नामालूम किन-किन हस्तियों के नाम पर स्थापित-घोषित होते पुरस्कारों या सम्मानों के पीछे कौन सा गणित काम कर रहा होता है! स्थानीय महाविद्यालयों की तो छोडिय़े ख्यात विश्वविद्यालयों में किन आधारों पर नियुक्तियां या पदोन्नतियां की जाती हैं, वह भी आये दिन बहसों में होता ही हैं।
यह सारे धतकरम केवल साहित्य में ही नहीं है, इतर विधाओं में भी ऐसी अनेक झंझटें हैं। बेशक इधर साहित्य-कला में अपने वक्त की असल चिंताओं या मानवीय मूल्यों के बरक्स फौरी समझौते ज्यादा महत्व पा रहे हैं। ऐसा मगर क्या राजनीति में नहीं हो रहा? क्या सामाजिक या इतर अकादमिक क्षेत्र इस बीमारी से बिलकुल मुक्त हैं? मूल्यों में आने वाले बदलाव किसी एक क्षेत्र या विधा को ही प्रभावित नहीं करतें। नैतिक पतन हर क्षेत्र को प्रभावित करता है।
कुछ बरस पहले कम्प्यूटर का चलन और प्रभाव बढऩे से चिंता व्यक्त की जाने लगी थी कि जल्द ही लिखित शब्द बीते वक्त की बात होगी! साहित्य गुजरे दौर की एक स्मृति मात्र होगा? आयातित का विरोध करने वाले कम्प्यूटर की मुखालिफत में तर्क गढ़ रहे थे। नवाचार के पक्षधर ठीक विपरित बातें करते। वक्त की कसौटी पर हर बहस का समाधान निकल आता है। न लिखित शब्द मरा है न तो साहित्य ही समाप्त हुआ है। पत्र-पत्रिकाएं छप रहे हैं। बेचे-खरीदे जा रहे हैं। बेशक ऑन-लाइन संस्करण भी चल पड़े हैं। वेब-पत्रिकाएं हैं। किताबों के डिजिटल संस्करण भी। किताबें तब भी बरकरार हैं। बिक रही हैं। संग्रहित की जा रही है। बदलते वक्त के बावजूद साहित्य बरकरार हैं। जोड़-तोड़, आत्म-प्रचार और दंद-फंद भरे इस समय में भी साहित्य-कला में, चाहे इने-गिने ही, ऐसे लोग भी है, जो इन बातों से दूर हैं। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
© 2017 - ictsoft.in

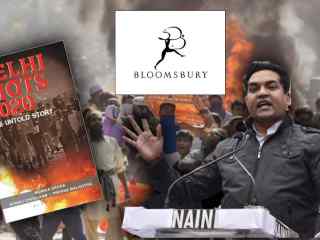






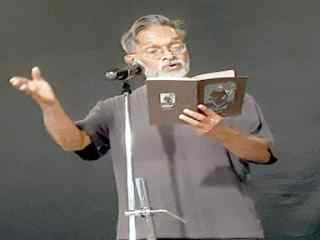








Leave a Comment